विषय प्रवेश -
लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल के माध्यम से ही लोकतंत्र संचालित होता हैैं। यह दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता हैं। लेकिन वर्त्तमान समय में लोगों की आवश्यकताएंँ एवं अपेक्षाएंँ इतनी बढ़ गयी है कि उन्हें पूरा करना अब राजनीतिक दलों के बस की बात नहीं रह गयी है। फलतः व्यक्ति अपनेे को समूहों व हित समूहों में गठित होने लगते हैं। ये समूह कई तरह के होते हैं, जैसे लाॅबीज, हित-समूह, गैर-सरकारी संगठन, अनौपचारिक संगठन, गुुट आदि इसके उदाहरण हैं। लेकिन उक्त सभी दबाव-समूह नहीं होते हैं। और न हित-समूह। वैसे तो प्रत्येक देश में हित-समूह व समाज में भी हित-समूह होते हैं। किंतु जब ये समूूह सत्ता को प्रभावित करने के इराद से राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं, तब वे दबाव-समूह बन जाते हैं।
अर्थ -
वस्तुतः दबाव समूह ऐसा माध्यम हैं जिसकेे द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करनेे का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह जो प्रशासनिक और संसदीय दोनों ही प्रकार के पदाधिकारियों को सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करनेे के लिए कोई प्रयत्न किये बिना ही प्रभावित करना चाहते हैं तो दवाब गुट की श्रेणी में आयेगे। दबाव-समूह की तुलना अज्ञात साम्राज्य से की जाती हैं, जब इनके हित संकट में होते हैं अथवा जब इन्हें कोई स्वार्थों की प्राप्ति करनी होती है तो वे सक्रिय बन जाते हैं। जब यह सक्रिय रहते हैंं तो दबाव-समूह और जब यह निष्क्रिय हो जाते हैं तो हित-समूह के रूप में रहते हैं अथवा माने जाते हैं।
परिभाषा -
दबाव-समूह की परिभाषा कई विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से दी हैं। कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाओं को हम निम्नलिखित ढंग से देखेंगे -
आडिगार्ड के अनुसार -
"दबाव-समूह वैसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य अथवा हित होते हैं और जो चीजों को विशेष रूप से करने का प्रयत्न करते हैंं जिससे कि वे अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि कर सकें।"
माइनर वीनर के अनुसार -
"दबाव- से हसमूहमारा तात्पर्य शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐसे ऐच्छिक, किन्तु संगठित समूह से है जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, उसके प्रशासन और समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता हैं।"
एच॰ जेगलर के अनुसार -
"दबाव-समूह एक संगठित समूह होता है जो सदस्यों को औपचारिक सरकारी पदों पर आसीन करवाने के प्रयास के बिना सरकारी निर्णयों के प्रसंग को प्रभावित करने का प्रयत्न करता हैं।"
फ्रांसिस कैसेल्स के अनुसार -
"दबाव-समूह का आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो शासकीय विधियों के माध्यम से या उनके बिना ही राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करता हैं।"
एल्फ्रेड जी॰ ग्रेजिया के अनुसार -
"दबाव-समूह एक ऐसा संगठित सामाजिक समूह है जो सरकार पर औपचारिक नियंत्रण किये बिना राजनीतिक अधिकारियों के व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास करता है।"
उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि दबाव समूह राजनीतिक दल से भिन्न होते हैं। यह एक प्रकार के हितों से सम्बद्ध लोगों का समूह होता हैं। अपने सदस्यों के हितों की साधना हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहता हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैधानिक तथा अवैधानिक अथवा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के तरीकों का प्रयोग करता हैं, जैसे- अनशन, धरना-प्रदर्शन, भूख हड़ताल, हड़ताल आदि। दबाव समूह शासन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लेता बल्कि शासन के विभिन्न अभिकरणों (एजेंसियों) को प्रभावित करता हैं।
अतः कहा जा सकता है कि दबाव समूह ऐसे समूह होते हैं जो अपने सदस्यों के हित साधन के लिए सरकार के विभिन्न अभिकरणों को वैधानिक या अवैधानिक तरीके से प्रभावित करते हैं।
दबाव समूहों का वर्गीकरण -
संगठन की दृष्टि से समूहों के दो भेद होते हैं -
- औपचारिक और
- अनौपचारिक।
औपचारिक समूह वे होते हैं जिनके गठन के किसी भी प्रकार का कोई नियम व विधान हो साथ-ही-साथ उसके कार्य प्रणाली निर्धारित हो। जिनके पास ये विधान व कार्य प्रणाली का अभाव होता हैं वे अनौपचारिक संगठन माने जाते हैं। समय व अवधि की दृष्टि से अल्पकालिक और दीर्घकालिक समूह होते हैं। इसी प्रकार कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी स्थानीय व व्यापक समूह होते हैं।
आज के परिप्रक्ष्य में देखते हैं तो पाते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के कुछ विद्वानों द्वारा दबाव समूहों का वर्गीकरण किया गया हैं, जिनमें दो वर्गीकरण प्रमुख रूप से माने जाते हैं -
- ब्लौण्डेल द्वारा वर्गीकरण और
- आमण्ड द्वारा वर्गीकरण।
ब्लौण्डेल ने दबाव समूहों का वर्गीकरण उनके निर्माण करने वाले तत्वों के आधार पर किया गया हैं। ब्लौण्डेल के अनुसार मुख्य रूप से दो प्रकार का दबाव समूह होते हैं -
- सामुदायिक दबाव समूह और
- संघात्मक दबाव समूह।
जिनके स्थापना के मूल में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध होते हैं, वे सामुदायिक दबाव समूह कहलाते हैं और जिनके स्थापना के मूल्य में किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति तत्व होते हैं, वे संघात्मक दबाव समूह कहलाते हैं। ब्लौण्डेल ने इनमें से प्रत्येक को दो भागों में विभाजित किया हैं। सामुदायिक दबाव समूह में रूढ़िगत एवं संघात्मक और संघात्मक दबाव समूह में संंरक्षणात्मक एवं उत्थानात्मक।
वही आमण्ड ने दबाव समूहों को हित समूह के नाम से पुकारते हुए इसकी चरित्रिक विशेषताओं को अपने वर्गीकरण का आधार बनाया हैं। आमण्ड के अनुसार ये समूूह चार प्रकार के होते हैंं -
- संस्थात्मक
- असंघात्मक
- प्रदर्शननात्मक या अनियमित और
- संघात्मक।
ब्लौण्डेल और आमण्ड का सामूहिक चार प्रकार का वर्गीकरण हैं। जिसे हम निम्नलिखित ढंग से अध्ययन करेंगे-
1. संस्थात्मक दबाव समूह -
इस प्रकार का दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमण्डलों, सेना, नौकरशाही, आदि में सक्रिय रूप से देखने को मिलता हैं। ये औपचारिक श्रेणी के दबाव समूह होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाशील रहते हैं और विभिन्न प्रकार के संस्थाओं की छत्रछाया में फलते-फूलते रहते हैं। ये अपने कल्याण की अभिव्यक्ति के साथ-साथ अन्य सामाजिक समुदायों के लिए भी क्रियाशील रहते हैं।
2. सामुदायात्मक (संघात्मक) दबाव समूह -
इनका मुख्य लक्ष्य अपने कल्याण की पूर्ति करना होता हैं, जैसे – व्यवसायिक संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, सरकारी कर्मचारियों का संगठन, छात्र संगठन, शिक्षक संगठन आदि।
3. असामुदायात्मक (असंघात्मक) दबाव समूह -
इस प्रकार के दबाव समूह धर्म, जाति, रक्त-संबंध आदि परंपरागत लक्षणों पर आधारित होते हैं। ये अनौपचारिक व असंगठित समूह होते हैं। आमतौर पर परम्परागत व संघात्मक संघात्मक समूहों को आधुनिक दबाव समूह भी कहा जाता हैं।
4. प्रदर्शनकारी (अनियमित) दबाव समूह -
इस प्रकार के दबाव समूह अपनी मांगों की पूर्ति के लिए गैर-संवैधानिक तरीकों को भी अपनाते हैं। जैसे – धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, भूख हड़ताल, जनसभाएं ,रैली, सत्याग्रह, अनशन, सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंँचाना, आत्मदाह, यातायात बाधित करना, घेेेराव आदि। कभी-कभी तो इनका आंदोलन हिंसात्मक भी हो जाता हैं, दंगे हो जाते हैं। इस प्रकार के कई तरह के आक्रमक रुख अपना कर अपनी मांगों की पूर्ति करवा भी लेते हैं। इन सबका उद्देश्य रहता है कि शासन पर दबाव बनाकर नीतियों को प्रभावित करके उद्देश्य की पूर्ति कराया जाय।
उपर्युक्त अध्ययन और वर्तमान सामाजिक सोच के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में असंघात्मक दबाव समूह सर्वाधिक प्रभावशाली है और इसमें भी जाति का उभार अधिक दिखता हैं। इसके बाद संस्थात्मक दबाव समूह राजनीति को अधिक प्रभावित किया है। अगर सामुदायात्मक दबाव समूह की बात करें तो पाते हैं कि केवल 'फेडरेशन ऑफ इंडिया, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री' को ही आधुनिक दबाव समूह माना जा सकता हैं।


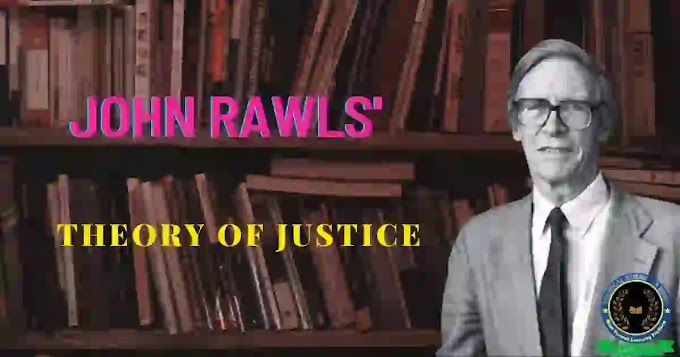
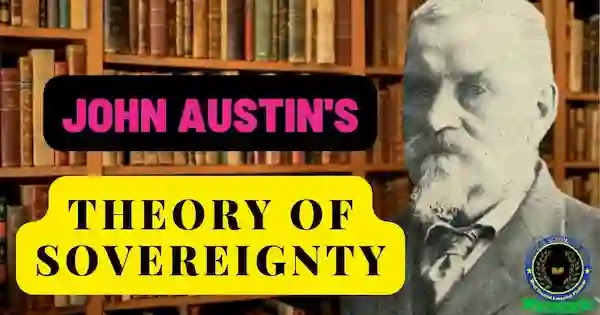
.webp)

0 टिप्पणियाँ
If you have any doubts, Please let me know