जब एक महिला को साक्षर किया जाता है तब एक परिवार साक्षर होता हैं। चूंँकि एक शिक्षित महिला शिक्षा के महत्व को समझते हुए, अपने बच्चों को भी शिक्षित करने के लिए प्रेरित व उत्साहित होती है और यहीं से किसी भी राष्ट्र में एक बेहतर मानव संसाधन का निर्माण की शुरुआत होने लगती हैं। समाज में महिला की स्थिति जितनी मजबूत होगी, समाज उतना ही विकसित व प्रभावपूर्ण होगा। धर्मग्रंथों में भी लिखा गया हैं- यत्र नार्मस्तु पूज्यते रमन्ते, तत्र देवता। इसके बावजूद भी महिला को अबला की संज्ञा देते हुए सदैव अपमानित व पद दलित किया जाता रहा हैैं। सदैव से यातना व शोषण की शिकार रही है महिलाएंँ। महिला की उन्नति के लिए विश्व स्तर पर पहली बार संगठित रूप से 1903 में अमेरिका में Women Trade Union गठित किया गया था। अमेरिका में 1910 में महिला दिवस मनाने का मुद्दा उठा था। शुरुआत में कई देश महिला दिवस अलग-अलग तिथियों में मनाया करते थे। बाद में एक तिथि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च निर्धारित कर दी गयी। तब से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' मनाया जाने लगा। जो अभी भी जारी हैं।
महिला सशक्तिकरण के लिए जब तक उन्हें आर्थिक स्तर पर सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक महिलाएंँ पुरुषों पर कमोबेश निर्भर रहने को बाध्य रहेंगी। इस पुरुष मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना आवश्यक हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा राज्य के पानीपत नामक शहर में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना की शुरुआत की थी। जो यह एक सामाजिक योजना हैं। इस योजना के माध्यम से लोगों में बेटियों के जन्म से संबंधित जो रूढ़िगत धारणा बन गयी थीं, उसे तोड़ना हैं। इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना भी लायी गयी। जिससे आर्थिक स्वरूप भी सुदृढ़ हो सकें। उक्त दोनों योजना को लाने का मुख्य कारण था कि भारत में बाल लिंगानुपात 1000 बेटों पर, बेटियों की संख्या 830 हैं। इतने बड़े अंतर को पाटने के लिए ही उक्त दोनों योजनाओं को लाना आवश्यक था। वैसे तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी व संवैधानिक स्तर पर कई प्रकार की पहल व प्रयास किये जाते रहे हैं।
आजादी के बाद महिलाओं की तस्वीर धीरे-धीरे हर कालखण्ड में बेहतर होती जा रही हैं। राजनैतिक व समजिक प्रतिबद्धता ने ऐसे वातावरण का निर्माण कर दिया है कि महिलाएंँ अपने को अब स्वतंत्र महसूस करने लगी हैं। महिलाओं से जुड़े विभिन्न उपबन्धों, अधिनियमों व योजनाओं ने उनके लिए जहांँ शिक्षा के नए अवसर प्रदान किए हैं वहीं रोजगार के नए-नए अवसर भी बढ़ाएंँ हैं। हर स्तर पर महिलाओं की क्षमताओं को आज स्वीकार भी किए जाने लगा हैं। इसका पूरा लबोलुआब यह है कि महिलाओं के दायित्वों की रूपरेखा भी नए परिवेश के साथ बदल रही हैं।
महिलाओं से जुड़े संवैधानिक उपबन्ध और अधिनियम -
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्य जो सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्रदान किए गये हैं। जिसमें महिला अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या भी हैं। इसी से महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार किया गया हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या लगभग 48.5 प्रतिशत हैं।
अब हम देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय संविधान में क्या-क्या व्यवस्था की गयी है जो निम्नलिखित हैं -
अनुच्छेद 14 - राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार एवं अवसर पर बल।
अनुच्छेद 15 - लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित।
अनुच्छेद 15 (3) - महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक दृष्टिकोण।
अनुच्छेद 16 - लोक नियोजन में अवसर की समानता।
अनुच्छेद 19 - विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 21 - प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 23 - बलात्, बेकार और दुर्व्यवहार की मनाही।
अनुच्छेद 24 - 14 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका के नियोजन की मनाही।
अनुच्छेद 39 - समान रूप से जीविका, समान वेतन एवं गरिमामय वातावरण का निर्माण।
अनुच्छेद 42 - काम की न्यायसंगत, मानवोचित दशाओं का निर्माण तथा प्रसूतिकाल में सहायता।
अनुच्छेद 47 - स्वास्थ्य एवं जीवन-स्तर में सुधार।
अनुच्छेद 51क (ड॰) - महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जारी प्रथाओं का त्याग एवं समरसता एवं भातृत्व की भावना का विकास।
अनुच्छेद 243 (घ) - पंचायतों में विभिन्न वर्गों की महिलाओं का आरक्षण।
अनुच्छेद 243 (न) - बिना भेदभाव नगरपालिकाओं में विभिन्न वर्गों की महिलाओं का आरक्षण।
अनुच्छेद 325 - भेदभाव बिना निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का अधिकार।
अनुच्छेद 226 - व्यस्क मताधिकार।
इन संवैधानिक उपबन्धों के अलावे महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिनियमों का प्रयोग औपनिवेशकाल से ही किया गया हैं। महिलाओं से जुड़ी सामाजिक कुरीतियों के दूर करने में शुरुआती दौर से देखें तो पाते हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), बाल विवाह निषेध अधिनियम (1925) और शारदा एक्ट (1929) अंग्रेजी शासन द्वारा भी क्रियान्वित किया जाता रहा हैं।
इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के बाद महिलाओं से जुड़ी कुरीतियों को दूर करने के लिए भी प्रयास किए गए। इन प्रयासों में हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), विशेष विवाह अधिनियम (1954), हिन्दु विवाह अधिनियम (1955), वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम (1956), हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम (1995), जो (2005) में संशोधित हुआ, कारखाना अधिनियम (1958) जो (1986) में संशोधित हुआ, दहेज निषेध अधिनियम (1961) जो (2012) में संशोधित हुआ, प्रसूति-प्रसुविधा अधिनियम (1961), भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम (1969), भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम (2001), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005), महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध और निवारण विधेयक (2012), महिलाओं के खिलाफ जघन्य यौन अपराध विधेयक (2013) और तीन तलाक अधिनियम (2019) को देख सकते हैं।
इसके अलावे में भी महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्पूर्ण विकास के लिए समय-समय पर कई प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता रहा हैं। जिसे हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं-
- कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल (1972-73)
- रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम (1986-87)
- स्वावलम्बन (1982-83)
- स्वयंसिद्धा (2001)
- राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति (2001)
- स्वधारा (2001-02)
- स्वर्णिम योजना (2002)
- महिला समाख्या योजना (1989)
- आशा योजना (2005)
- बालिका समृद्धि योजना (1997)
- स्वशक्ति (1998)
- अल्पावधि प्रवास गृह (1969)
- परिवार परामर्श केंद्र (1984)
- निःशुल्क बालिका शिक्षा (इंदिरा गांधी इकलौती बालिका छात्रवृति योजना) (2005)
- बालिका प्रोत्साहन योजना (2006-07)
- किशोरी शक्ति योजना (2001)
- राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (2001)
- महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना (2001)
- जननी सुरक्षा योजना (2005)
- जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना (2003)
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (2004)
- महिला डेयरी विकास परियोजना (2004)
- वंदेमातरम् योजना (2004)
- मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (2003)
- जेंडर बजटिंग (2004-05)
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (2008)
- चलो गांँव की ओर कार्यक्रम (2006)
- उज्ज्वला योजना (2007)
- धनलक्ष्मी योजना (2008)
- राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम (2010-11)
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (2010-11)
- महिला के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन (2010)
- महिला किसान सशक्तिकरण योजना (2010)
- प्रियदर्शनी (2010)
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (2011)
- स्त्री शक्ति पुरस्कार (1999)
इसके अतिरिक्त भी महिला के उत्थान के लिए 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग और 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। ताकि महिला के विकास में वित्तीय संकट उत्पन्न न हो।
उपर्युक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि आजादी से पहले व आजादी के बाद से ही महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास किया जाता रहा हैं। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहांँ महिलाएं अपनी उपस्थिति का आभास न करा रही हो। महिलाओं के प्रति पुरुषों के नजरियों में भी बदलाव आया हैं। चाहे वह सरकारी व गैर-सरकारी स्तर ही क्यों न हो। अब महिलाएंँ निर्णयों में केन्द्रीय भूमिका निभा रही हैं। महिला अधिकारों ने ऐसी प्रक्रिया को जन्म दे दिया है जिसमें वे संगठित होकर अपने सतत् विकास को प्राप्त कर रही हैं। पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होने से सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रवेश का अवसर प्राप्त हुआ हैं। महिलाएंँ पंचायत से लेकर संसद तक में अपनी उपस्थिति दमदार तरीके से दर्ज करा रही हैं। महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण तो मिल गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर देश की पंचायत (संसद) में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण अभी तक पारित नहीं हो सका हैं। हो सकता है कि पुरुष मानसिकता के कारण ऐसा न हो पाया हो। क्योंकि यह भी चिंता स्वीकार करने योग्य हो कि जिस तरह से महिलाओं के लिए काम होते जा रहा हैं। मातृसत्तात्मक की ओर ले जाता हुआ दिख रहा हो भय भी हो सकता है कि कहीं पुरुष हाशिये पर न चला जाए।
फिर भी यह सच्चाई है कि महिला अधिकार और सशक्तिकरण भारतीय समाज की आवश्यकता हैं। क्योंकि किसी वर्ग को दबाकर विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता हैं। चाहे वह वर्ग महिला हो या पुरुष। महिलाएंँ भी हमारे समाज की हिस्सा हैं, उनकी तरक्की को किसी भय व शंका के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों वर्गों का दायित्व एक-दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।


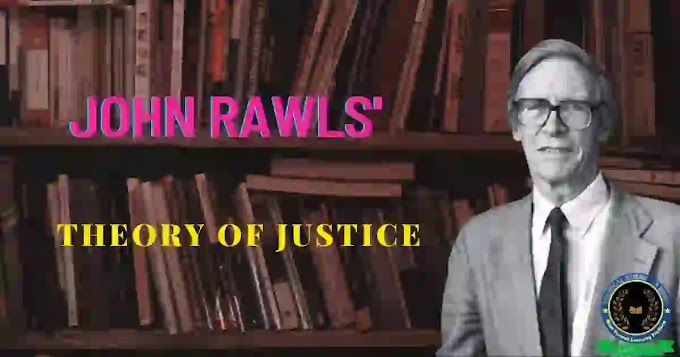
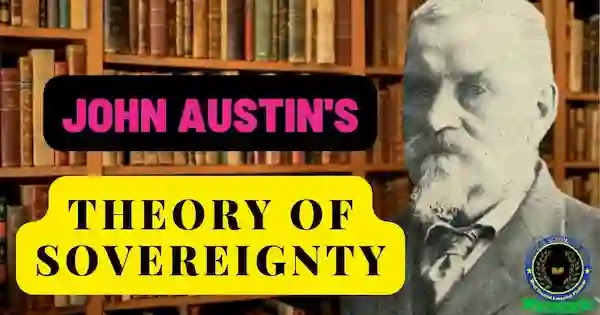
.webp)

0 टिप्पणियाँ
If you have any doubts, Please let me know